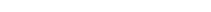Feed aggregator
India-New Zealand: Free trade talks relaunched after a decade - BBC.com
- India-New Zealand: Free trade talks relaunched after a decade BBC.com
- Watch: New Zealand PM's Champions Trophy final quip leaves PM Modi in splits India Today
- PM Modi hopes New Zealand government will act against anti-India actors The Economic Times
- 'Avoid diplomatic incident': Luxon thanks PM Modi for not mentioning NZ's Champions Trophy defeat The Times of India
- PM Modi Raises Concerns Over Pro-Khalistani Activities With New Zealand PM NDTV
HP launches AI-enhanced EliteBook laptops for enterprises: Price, features - Business Standard
- HP launches AI-enhanced EliteBook laptops for enterprises: Price, features Business Standard
- HP Launches AI-powered EliteBook Ultra G1i, EliteBook X G1i, and EliteBook X G1i Flip with Intel Core Ult The Times of India
- HP launches new commercial AI PCs featuring Intel and AMD processors in India The Hindu
- HP launches new AI-powered EliteBook laptops in India Moneycontrol
- HP’s latest commercial PCs offer up to 55 TOPS of AI performance The Indian Express
CAG नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठे सवाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति के नियमों में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
याचिका में राष्ट्रीय लेखा परीक्षक चुनने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर एक पैनल बनाने की मांग की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
महाराष्ट्र में सीएजी के ऑडिट रोके जा रहे: याचिकाकर्तासुनवाई के दौरान एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष दलील दी कि 'संस्था की स्वतंत्रता' का सवाल है। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीएजी द्वारा ऑडिट रोके जा रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है। हाल के दिनों में सीएजी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। पीठ ने उनसे हाल के वर्षों में सीएजी की स्वतंत्रता पर संदेह करने के कारण को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा।
प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि सीएजी की रिपोर्ट कम हो रही है। कर्मचारियों की संख्या घट रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के संबंध में हस्तक्षेप किया था, ताकि उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। प्रशांत भूषण ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सीएजी के लिए भी इसी तरह के निर्देश आवश्यक हैं।
याचिकाकर्ता ने क्या की मांग?याचिका में कहा गया कि न्यायालय यह निर्देश दे कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक स्वतंत्र और तटस्थ चयन समिति के परामर्श से और पारदर्शी तरीके से की जाए। वहीं, सीएजी की नियुक्ति का निर्देश सूचना आयोगों और केंद्रीय सतर्कता आयोग सहित अन्य निकायों की नियुक्ति के समान होना चाहिए।
क्या काम करता है सीएजी?नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित/समीक्षा करता है।
यह भी पढ़ें: क्या AAP की बढ़ेंगी और मुश्किलें? आज सदन में पेश की जाएगी CAG की दूसरी रिपोर्ट
डिप्रेशन और कैंसर... वापसी के बाद भी आसान नहीं होगी सुनीता विलियम्स की जिंदगी; किन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Sunita Williams News नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए स्पेसएक्स का क्रू-10 मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। वहां पहुंचने पर नए सदस्यों का स्वागत किया गया।
अब अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीद जगी है।
सुनीता विलियम्स (Sunita Williams News) व बुच विलमोर जून 2024 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर फंसे हैं। दोनों 8 दिनों के लिए ही स्पेस में गए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के चलते दोनों 284 दिनों तक वहां फंसे रहे।
स्पेस में इतने लंबे समय तक रहने के कई खराब असर भी होते हैं, आइए जानते हैं आखिर इससे शरीर पर क्या असर होता है....
शरीर पर क्या पड़ता है प्रभाव ?- अंतरिक्ष में ग्रैविटी न होने और तेज विकिरण (रेडिएशन) अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं।
- लंबे समय तक स्पेस में रहने के चलते हड्डियों में कमजोरी, मांसपेशियों में सिकुड़ना, आंखों की रौशनी कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- स्पेस में जाकर अक्सर वजन कम नहीं होता, लेकिन ग्रैविटी की कमी की वजह से शरीर में बदलाव आते हैं। माइक्रोप्रैविटी से शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की ओर खिसकते हैं, जिससे चेहरा सूजा हुआ लग सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्री पतले दिख सकते हैं।
- सुनीता ने बताया कि उनका वजन अंतरिक्ष में पहले जितना ही है।
धरती पर वायुमंडल व चुंबकीय क्षेत्र (मैग्नेटिक फिल्ड) हमें रेडिएशन से बचाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में रेडिएशन का ज्यादा असर होता है। इससे डीएनए को नुकसान होता है, जिससे कैंसर व तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है।
मेंटल हेल्थ पर कितना असर?अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। डिप्रेशन, तनाव और चिंता का खतरा बढ़ना आम है। अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर धरती पर वापस आने पर साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है।
You’ve heard of the Big Bang. Now astronomers have discovered the Big Wheel – here’s why it’s significant - The Conversation
- You’ve heard of the Big Bang. Now astronomers have discovered the Big Wheel – here’s why it’s significant The Conversation
- A giant disk galaxy two billion years after the Big Bang Nature.com
- ‘Cosmic monster alert’: 11-billion-year-old galaxy too big for science to explain Business Today
- 8 Most Stunning Space Photos Taken By NASA James Webb Telescope Times Now
- James Webb Space Telescope's First Deep Field Image Is Mind-Boggling MSN
Tirumala to accept Telangana recommendation letters - Deccan Chronicle
- Tirumala to accept Telangana recommendation letters Deccan Chronicle
- TTD to accept recommendation letters of public representatives of Telangana from March 24 The Hindu
- TTD to accept recommendation letters of elected leaders from Telangana starting March 24 The Times of India
- TTD to accept recommendation letters from Telangana public representatives Telangana Today
- TTD Announces Special Darshan Facility for Telangana Public Representatives ap7am
FC Barcelona News: 17 March 2025 - Barca Blaugranes
- FC Barcelona News: 17 March 2025 Barca Blaugranes
- Atletico comeback shows Hansi Flick’s Barcelona is a team that refuses to lose Barca Blaugranes
- Watch: Lamine Yamal scores in 93rd minute as Barcelona further Atletico Madrid heartbreaks The Times of India
- Barcelona come back at Atletico Madrid to claim LaLiga top spot Al Jazeera English
- Robert Lewandowski matches remarkable Lionel Messi feat after scoring crucial goal for Barcelona in comeback win over Atletico Madrid GOAL English
आधार कार्ड के नाम पर मुंबई की 86 वर्षीय महिला के साथ बड़ा स्कैम! डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 20 करोड़ रुपये
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आए दिन साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई है, जहां एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से जालसाजों ने 20.25 करोड़ रुपये की ठगी कर ली।
कैसे हुई महिला के साथ ठगी?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 26 दिसंबर 2024 से लेकर 3 मार्च 2025 तक महिला को लगातार ठग फोन कर रहा था। ठग ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि महिला का आधार कार्ड गलत कामों में इस्तेमाल हो रहा है। ठग द्वारा महिला को काफी ज्यादा डराया गया।
जालसाजों ने महिला को बताया कि उसके नाम से नया बैंक अकाउंट खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैरकानूनी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। ठगों ने महिला के साथ-साथ उनकी बेटी को भी फंसाने की धमकी दी। इसके बाद ठगों ने महिला को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और मामले को खत्म करने के लिए पैसे भेजने को कहा।
महिला को किया गया 'डिजिटल अरेस्ट'
जालसाजों ने महिला से कहा कि वो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताए, क्योंकि वो डिजिटल अरेस्ट में है। इसके बाद महिला ने डर से अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब महिला को शक हुआ, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर ठगों को ट्रैक कर लिया।
ईडी अफसर बनकर ठगों ने की थी ठगी
जालसाज प्रवर्तन अधिकारी या सरकारी एजेंट बनकर, कठोर लहजे और फर्जी फोन नंबरों का इस्तेमाल करके अपने शिकार से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करते हैं। एक वरिष्ठ साइबर सेल अधिकारी ने बताया, "जैसे-जैसे पीड़ित की डर बढ़ता जाता है, ठग अपने कार्यों में हेरफेर करके दायित्व की झूठी भावना पैदा करने का अवसर प्राप्त करते हैं।"
यह घोटाला आम तौर पर एक घोटालेबाज के फोन कॉल या मैसेज से शुरू होता है, जिसमें दावा किया जाता है कि पीड़ित के पास एक बकाया वारंट या उसके पार्सल में ड्रग्स है और गिरफ्तारी या आगे की सजा से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
वे अपने फोन नंबर को छिपाने के लिए स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कॉल किसी वैध सरकारी एजेंसी से आ रही है। जैसे-जैसे पीड़ित अधिक चिंतित और भयभीत होता जाता है, घोटालेबाज व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी निकालना शुरू कर देता है। वे प्रीपेड डेबिट कार्ड, वायर ट्रांसफर या अन्य अप्राप्य तरीकों से भुगतान मांग सकते हैं।
डिजिटल अरेस्ट और स्कैम से कैसे बचें?
ध्यान रखें कि न तो पुलिस और न ही UIDAI के अधिकारी कभी भी पर्सनल डिटेल्स, OTP या डिवाइस का रिमोट एक्सेस मांगते हैं। आपको ऐसा कोई कॉल आए, तो तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें। इसके बाद UIDAI के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर इसकी सूचना दें।
Digital Arrest के खिलाफ सरकार का एक्शन, 83 हजार वॉट्सऐप अकाउंट बंद, करोड़ों का नुकसान भी बचा
न्यूजीलैंड और भारत मिलकर करेंगे आतंक का सफाया, पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आगे का प्लान
एएनआई, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आतंकवाद पर हमारी राय एक जैसी है। चाहे 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च पर हुआ आतंकी हमला हो या मुंबई 26/11, आतंकवाद हर तरह से अस्वीकार्य है।
उन्होंने कहा, आतंकी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हम आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे।
#WATCH | Delhi: During the joint press statement with New Zealand PM Christopher Luxon, PM Modi says, "We have the same opinion on terrorism. Whether it is the terror attack on Christ Church on March 15, 2019, or Mumbai 26/11, terrorism is unacceptable in every manner. Strict… pic.twitter.com/ZhyYotf4ur
— ANI (@ANI) March 17, 2025पीएम मोदी ने कहा, हमने न्यूजीलैंड में भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता साझा की है। हमें यकीन है कि हमें इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ न्यूजीलैंड सरकार की सहायता मिलती रहेगी"
इससे पहले, दोनों प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक भी की। लक्सन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री लक्सन और उनके मंत्रिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री लक्सन भारत से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि उन्होंने हाल ही में होली कैसे मनाई। हमें खुशी है कि उनके जैसे युवा नेता रायसीना डायलॉग 2025 में हमारे मुख्य अतिथि हैं।"
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "अवैध प्रवास के मुद्दे से निपटने के लिए भारत और न्यूजीलैंड द्वारा एक समझौता तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा।"
Justice Joymalya Bagchi: कौन हैं जस्टिस बागची, जो बने सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज; 2031 में संभालेंगे CJI का कार्यभार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक समारोह आयोजित कर जस्टिस बागची को शपथ दिलाई गई है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहे।
न्यायमूर्ति बागची के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के साथ ही अब शीर्ष अदालत में 33 न्यायाधीश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। फिलहाल एक पद खाली है। बता दें, जस्टिस बागची का कार्यकाल 6 साल से अधिक का होगा। इस दौरान वो सीजेआई का भी पदभार संभालेंगे।
पांच महीने तक संभालेंगे सीजेआई का पद
न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची न्यायाधीश केवी विश्वनाथन के बाद सीजेआई का पद संभालेंगे। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन 25 मई 2031 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद संभालेंगे।
केंद्र ने 10 मार्च को दी थी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 10 मार्च को न्यायमूर्ति बागची के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की मंजूरी दी थी। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने 6 मार्च को उनके नाम की सिफारिश की थी। इस कॉलेजियम में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल थे।
कॉलेजियम ने क्या कहा?
कॉलेजियम ने कहा था कि 18 जुलाई 2013 को न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्ति के बाद से कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत का प्रधान न्यायाधीश नहीं बना है। जस्टिस बागची को 27 जून 2011 को कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 4 जनवरी 2021 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।
कलकत्ता में 13 वर्षों से अधिक तक किया काम
जस्टिस बागची को आठ नवंबर 2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया था और तब से वो वहीं कार्यरत थे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 13 साल से अधिक समय तक कार्य किया है।
RG Kar Case: आरजी कर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पीड़िता के परिवार को जगी उम्मीद
Dummy Models of iPhone 17 Lineup Reveal New Camera Bump Design, MagSafe Support - Deccan Chronicle
- Dummy Models of iPhone 17 Lineup Reveal New Camera Bump Design, MagSafe Support Deccan Chronicle
- Elon Musk replies to video of Joe Rogan taking delivery of custom Tesla Model S Plaid The Times of India
- iPhone 17 Air nearly ditched charging port to become the slimmest, dummy images reveal MagSafe India Today
- iPhone 17 Air to feature razor-thin design; will it be the slimmest iPhone ever? Moneycontrol
- iPhone 17 Pro Max replacement launching soon - know 5 things about Ultra model Hindustan Times
Data Decode : जलवायु परिवर्तन से जीडीपी और कृषि को खतरा, एक डिग्री तापमान बढ़ने पर 12% की गिरावट का अनुमान, मक्का, गेहूं और धान सबसे अधिक प्रभावित
नई दिल्ली, अनुराग मिश्र/विवेक तिवारी
बीते एक दशक में जलवायु परिवर्तन से चरम मौसम की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से गर्मी, सर्दी और बारिश में अनियमितता बढ़ी है। इसका प्रभाव जहां एक तरफ आपदाओं की घटना में बढ़ोतरी के तौर पर पड़ा है तो दूसरी तरफ शारीरिक और आर्थिक क्षति में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि एक डिग्री तापमान बढ़ने पर पूरी दुनिया की जीडीपी में 12 फीसदी तक की कमी देखी जाएगी। इसके अलावा बारिश में कमी होने का फर्क उत्पादकता और पोषण में भी देखने में आ रहा है। प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों का विस्थापन भी बढ़ा है।
बढ़ती गर्मी का असर जीडीपी पर
आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि एक डिग्री तापमान बढ़ने पर पूरी दुनिया की जीडीपी में 12 फीसदी तक की कमी देखी जाएगी। वहीं एडवांसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंस नामक एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संघ ने अपने अध्ययन में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति वर्ष तीन प्रतिशत तक घट सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए लिए समावेशी और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे संवेदनशील देश है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की संवेदनशीलता को देखते हुए, एक मजबूत रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 22 के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7 प्रतिशत से 5.6 प्रतिशत तक की वृद्धि विकास रणनीति में अनुकूलन और लचीलापन निर्माण की प्रमुख भूमिका को दर्शाती है। ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के निदेशक डॉ. ध्रुबा पुरकायस्थ कहते हैं कि "आर्थिक सर्वेक्षण भारत की एक मजबूत समग्र आर्थिक स्थिति की तस्वीर पेश करता है। निरंतर वृद्धि, कम चालू खाता घाटा, सुव्यस्थित पूंजीकृत बैंकिंग सिस्टम और स्थिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल निर्माण सहित प्रमुख संकेतक इस मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी संरचनात्मक बदलाव देश को एक विकसित देश 'विकसित भारत' बनने की दिशा में आगे बढ़ने में अतिरिक्त रूप से मददगार हैं। इस सकारात्मक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, भारत 2030 से पहले अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर कर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक अच्छी स्थिति में है। आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिया जाना सामयिक और प्रासंगिक है। विशेष तौर पर, जलवायु से संबंधित आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता को देखते हुए। उम्मीद है कि बजट में भी इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ नीतियों पर बात होगी।
कॉर्बन उत्सर्जन में आ रही कमीआर्थिक सर्वे के मुताबिक देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन पुरी दुनिया के मुकाबले कम है, ये दिखाता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि, अक्षय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। खासकर ऊर्जा के भंडारण, प्रौद्योगिकी की कमी और खनिजों तक पहुंच की चुनौतियों के चलते हालात कई बार मुश्किल हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की संवेदनशीलता को देखते हुए, एक मजबूत रणनीति बेहद आवश्यक है। वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 22 के बीच जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7 प्रतिशत से 5.6 प्रतिशत तक की वृद्धि विकास रणनीति में अनुकूलन और लचीलापन निर्माण की प्रमुख भूमिका को दर्शाती है। वहीं इस बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड का प्रवाह काफी अपर्याप्त रहा है। देश में इस दिशा में ज्यादातर काम घरेलू संसाधनों की मदद से किया जा रहा है। हाल ही में CoP29 के परिणाम इस मामले में बहुत कम आशाजनक हैं।
एनआरडीसी इंडिया के लीड, क्लाइमेट रेजिलिएंस एंड हेल्थ अभियंत तिवारी कहते हैं कि डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि आने वाले सालों में मुश्किल काफी बढ़ने वाली है। क्लाइमेट चेंज के चलते गर्मी के साथ ही आर्द्रता का स्तर भी बढ़ रहा है। इसके चलते हीट स्ट्रेस की स्थिति तेजी से बढ़ी है। सामान्य तौर पर 35 डिग्री से ज्यादा तापमान और हवा में उच्च आर्द्रता होने पर लोगों को सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में हीट स्ट्रेस की स्थिति बनती है। बढ़ती हीटवेव जैसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से अर्ली वॉर्निंग सिस्टम भी तैयार किया गया है। जिसके आधार पर सरकार उचित कदम उठाने के लिए अलर्ट जारी करती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये सूचनाएं समय रहने सभी जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच सकें और वो उचित कदम उठाएं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चिंता क्लाइमेट चेंज के चलते तापमान में आ रहा बदलाव के चलते बढ़ता बीमारियों का खतरा है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ों के ठंडे मौस के चलते वहां पहले मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां नहीं होती थीं। लेकिन वहां जलवायु परितर्वन के चलते तापमान बढ़ा और अब ये स्थिति हो रही है कि मच्छरों को पनपने के लिए वहां बेहतर पर्यावरण मिल रहा है। इससे वहां मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ी हैं। इस तरह की मुश्किलों को देखते हुए हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को भी और मजबूत करना होगा। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कदम उठए जा सकें।
बढ़ती गर्मी का मक्का, गेहूं, धान पर सबसे ज्यादा असरबिहार कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर फिजा अहमद कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने कृषि पर बड़ा प्रभाव डाला है। इससे मक्का जैसी फसल हर हाल में प्रभावित होगी क्योंकि वे तापमान और नमी के प्रति संवेदनशील हैं। उनके अनुमान के मुताबिक 2030 तक मक्के की फसल के उत्पादन में 24 फीसदी तक गिरावट की आशंका है। गेहूं भी इसकी वजह से काफी प्रभावित हो रहा है। वह बताते हैं कि अगर तापमान में चार डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो गया तो गेहूं का उत्पादन पचास फीसद तक प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा धान की पैदावार में भी गिरावट आ सकती है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्रॉप साइंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ. टी.आर.शर्मा कहते हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो असर हमारी थाली पर पड़ेगा। अगर हमें अपने खाने और फसलों को बचाना है तो अनुसंधान पर लगातार खर्च करना होगा। डॉ. शर्मा कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर हर फसल पर पड़ रहा है। ठंड ज्यादा पड़ रही है, बारिश असमान हो रही है, इसका साफ असर फसलों पर देखने में आ रहा है। फसलों में नई-नई बीमारियां क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। बीते कुछ सालों में धान और मक्का की फसल पर इसका प्रभाव पड़ा है। हाल में हुई अधिक बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में धान की काफी फसल बर्बाद हुई।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश के 573 ग्रामीण जिलों में जलवायु परिवर्तन से भारतीय कृषि पर खतरे का आकलन किया है। इसमें कहा गया है कि 2020 से 2049 तक 256 जिलों में अधिकतम तापमान 1 से 1.3 डिग्री सेल्सियस और 157 जिलों में 1.3 से 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। इससे गेहूं की खेती प्रभावित होगी। गौरतलब है कि पूरी दुनिया की खाद्य जरूरत का 21 फीसदी गेहूं भारत पूरी करता है। वहीं, 81 फीसदी गेहूं की खपत विकासशील देशों में होती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट रिसर्च के प्रोग्राम निदेशक डॉ. पीके अग्रवाल के एक अध्ययन के मुताबिक तापमान एक डिग्री बढ़ने से भारत में गेहूं का उत्पादन 4 से 5 मीट्रिक टन तक घट सकता है। तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने पर उत्पादन 19 से 27 मीट्रिक टन तक कम हो जाएगा। हालांकि बेहतर सिंचाई और उन्नत किस्मों के इस्तेमाल से इसमें कमी की जा सकती है।
मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोमेट्रोलॉजी डॉक्टर मनीष भान कहते हैं कि एक दशक पहले तक मार्च महीने में तापमान बढ़ना शुरू होते थे। इससे गेहूं की फसल को पकने में मदद मिलती थी। वहीं पिछले कुछ सालों में फरवरी में ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गेहूं में दाने बनने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। दाने छोटे रह जाते हैं और उत्पज घट जाती है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंफ्रो कॉप मॉडल और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के डिसिजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नॉलिजी ट्रांस्फर दोनों बताते हैं कि 2025 तक औसत तापमान डेढ़ डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे 120 दिन वाली गेहूं की फसल 100 दिन में ही तैयार हो जाएगी। इससे दानों को मोटा होने का समय ही नहीं मिलेगा। गर्मी बढ़ने से पौधे में फूल जल्दी आ जाएंगे। ऐसे में फसल को दाना छोटा हो जाएगा और फसलें 120 दिन वाली फसल 100 दिन में ही तैयार हो जाएगी।
हर दशक औसत 1.22% घट रही मानूसन की बारिश, फसलों के लिए बढ़ा संकटमौसम विभाग (IMD) के जर्नल मौसम में हाल में ही छपे एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हर दशक में बारिश के दिनों में औसतन 0.23 फीसदी कमी दर्ज की गई है। ध्ययन के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक देश में बारिश का समय लगभग डेढ़ दिन कम हो गया है। यहां बारिश के एक दिन का मतलब ऐसे दिन से है जिस दिन कम से कम 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले एक दशक में एक्सट्रीम इवेंट्स भी काफी तेजी से बढ़े हैं।
आईएमडी जर्नल मौसम में प्रकाशित ये अध्ययन 1960 से 2010 के बीच मौसम के डेटा के आधार पर किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि बारिश के लिए जिम्मेदार लो क्लाउड कवर देश में हर दशक में लगभग 0.45 फीसदी कम हो रहा है। खास तौर पर मानसून के दिनों में इनमें सबसे ज्यादा, 1.22 प्रतिशत कमी आई है। मौसम विभाग के अध्ययन के मुताबिक 1971 से 2020 के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण पश्चिम मानसून देश की कुल बारिश में लगभग 74.9 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। इसमें से जून महीने में लगभग 19.1 फीसदी बारिश होती है। वहीं जुलाई में लगभग 32.3 फीसदी और अगस्त में लगभग 29.4 फीसदी बारिश होती है। सितंबर महीने में औसतन 19.3 फीसदी बारिश दर्ज की जाती है।
जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी और बारिश में लगातार हो रही कमी भारतीय कृषि के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हाल ही में हुए अध्ययनों से ये सामने आया है कि बारिश की कमी और कृषि उपज के बीच गहरा संबंध है। मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक पिछले लगभग दो दशकों में बारिश में काफी कमी आयी है। ऐसे में आने वाले समय में फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट का खतरा है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए, विशेषज्ञों ने अगले कुछ दशकों में तापमान और वर्षा में बदलाव के संभावित प्रभावों को लेकर चेतावनी दी है। ऐसे में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने और कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही है। वहीं ऐसी फसलों के विकास पर जोर दिया है जो ज्यादा कर्मी सह सकें और जिन्हें कम पानी की जरूरत हो।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कई अध्ययनों में साफ हो चुका है कि बारिश की कमी फसलों के उत्पाद को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। दिग्विजय सिंह नेगी और भारत सामास्वामी की रिसर्चगेट में छपि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश में कमी और बढ़ती गर्मी के चलते 2099 तक वार्षिक तापमान में 2° तक की वृद्धि देखी जा सकती है, वहीं बारिश में 7 फीसदी की बढ़ोतरी से कृषि उत्पादकता में 8-12% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमें बेहतर सिंचाई के संसाधनों के विकास के साथ ही गर्मी, सूखे और बाढ़ जैसे हालात में उपज देने वाली फसलों का विकास अनिवार्य हो गया है। आईसीएआर की संस्था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह कहते हैं कि पिछले एक दशक में हम देखें तो बारिश के सीजन में कमी नहीं आई है लेकिन बारिश के दिनों में कमी आ गई है। पहले जहां हमें बारिश के तीन महीनों में 72 दिनों तक बारिश मिल जाती थी वहीं अब इनकी संख्या घट कर 42 हो गई है। ऐसे में इन दिनों में कई बार हमें अचानक और बहुत तेज बारिश देखने को मिलती है। इसके चलते फसलों को नुकसान पहुंचता है। बदलते मौसम को देखते हुए तमान तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे उत्पादन पर असर न हो। सबसे पहले तो किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो फसलों के बुआई के समय, गर्मी और ज्यादा बारिश बरदाश्त कर सकने वाली फसलों, और फर्टलाइजर मैनेजमेंट के प्रति जागरूक हों। वहीं वैज्ञानिक लगातार ऐसी फसलों के विकास में लगे हैं जो जलवायु परिवर्तन को बर्दाश्त कर सकें। इसके अलावा ऐसी फसलों के विकास पर काम किया जा रहा है जिनकी बुआई के समय में लचीलापन हो। बारिश और गर्मी के आधार पर इनकी बुआई के समय बदलाव किया जा सके। वहीं बारिश के पैटर्न में बदलाव को देखते हुए एग्रोनॉमी तकनीकों को भी विकसित किया जा रहा है। वहीं मौसम में बदलाव को देखते हुए जमीन के आर्गेनिक कार्बन को बचाए रखने के लिए फसलों के अवशेष को खेतों में सड़ानें, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने आदि का भी काम किया जा रहा है। हालात को देखते हुए पहले ही लगभग 650 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया जा चुका है। वहीं अब ब्लॉक आधार पर भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। आपात स्थित में इनके आधार पर किसानों को बेहतर फसल के लिए जागरूक किया जा सकेगा।
कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते देश के कई इलाकों में कभी भारी बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। हाल ही में सरकार ने जलवायु परिवर्तन को देखते हुए 109 नई उन्नत प्रजातियों के बीज मार्केट में उतारे हैं। अब फसलों की इस तरह की प्रजातियां तैयार की जा रही हैं कि एकदम से सूखा या बाढ़ की स्थति बने तो भी हमें कुछ उत्पादन मिलता रहे। फसल पूरी तरह से खत्म न हो। वहीं अनाज में पोषण की मात्रा को भी बढ़ाया जा सके। आज भी देश में एक ऐसा वर्ग है जो पोषण के लिए सिर्फ खाद्यान पर निर्भर है। जैव संवर्धित बीज इन लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं।
जून से सितंबर के बीच होती है इस तरह बारिश
मौसम विभाग के अध्ययन के मुताबिक 1971 से 2020 के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण पश्चिम मानसून देश की कुल बारिश में लगभग 74.9 फीसदी की हिस्सेदारी रहती है। इसमें से जून महीने में लगभग 19.1 फीसदी बारिश होती है। वहीं जुलाई महीने में लगभग 32.3 फीसदी और अगस्त महीने में लगभग 29.4 फीसदी बारिश होती है। सितंबर महीने में औसतन 19.3 फीसदी बारिश दर्ज की जाती है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 तक 1.4 करोड़ भारतीयों ने छोड़ा घर, 2050 तक 4.5 करोड़ होंगे बेघर
‘कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इनएक्शन:डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन’ रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम से जुड़ी आपदाओं की वजह से 2050 तक 4.5 करोड़ भारतीय अपनी जगहों से विस्थापित हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सूखा, समुद्री जलस्तर के बढ़ने, जल संकट, कृषि और इको-सिस्टम को हो रहे नुकसान के चलते लोग विस्थापन को मजबूर हैं।
2030 तक 22.5 मिलियन लोग विस्थापित हो जाएंगेकॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इनएक्शन:डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन रिपोर्ट में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल किया गया है। बांग्लादेश में घाटों से नदी का कटाव, भारत और पाकिस्तान में बाढ़, नेपाल में पिघलते ग्लेशियर, भारत और बांग्लादेश में उफनते समुद्र, श्रीलंका में चावल और चाय के बागान वाले इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा और साइक्लोन इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका की वजह से घर, संपत्ति, बिजनेस, समुदाय आदि तबाह होते जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई मौसम की अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से हर साल जान-माल का नुकसान होता है।
स्टडी इस ओर इंगित करता है कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया का मौसम और खराब हो सकता है। यहां असहनीय हीटबेव, गंभीर सूखा, समुद्र का बढ़ता स्तर और साइक्लोन जैसी घटनाएं होंगी। आंकड़े बताते हैं कि इन पांच देशों में अगर पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य हासिल होता है, तो 2030 तक 22.5 मिलियन लोग विस्थापित हो जाएंगे और 2050 तक 34.4 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। गौरतलब है कि इन आंकड़ों में बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं से होने वाले विस्थापन को नहीं जोड़ा गया है, वरना यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा होता, क्योंकि ये देश बड़े पैमाने पर बाढ़ और तूफान जैसी अचानक आने वाली त्रासदियों का दंश झेल रहे हैं।
2020 में मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा की गई एक रिसर्च इस बात की तसदीक करती है कि यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 2050 तक दक्षिण एशियाई देशों को अपनी जीडीपी का 2 फीसदी नुकसान होगा। यह नुकसान उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और सदी के अंत तक बढ़कर 9 फीसदी हो जाएगा। इसमें जलवायु से जुड़ी चरम आपदाओं से होने वाले नुकसान को नहीं जोड़ा गया है, वरना यह आंकड़ा इससे कहीं अधिक होता। क्या है वजह रिपोर्ट के अनुसार, अब तक हुए उत्सर्जन में दक्षिण एशिया का 5 फीसदी से कम हिस्सा रहा है, जबकि वह दुनिया की एक चौथाई आबादी का घर है, जो बड़े पैमाने पर जलवायु से जुड़ी आपदाओं जैसे- बाढ़, सूखा, तूफान आदि का असर झेल रही है। 1990 से 2015 के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया के 10 फीसदी अमीरों ने करीब 52 फीसदी उत्सर्जन किया था। जबकि इसके विपरीत गरीब तबके की 50 फीसदी आबादी केवल 7 फीसदी उत्सर्जन के लिए उत्तरायी है। रिपोर्ट के अनुसार, 1998 से 2017 तक भारत को भूकंप, सुनामी, तूफान, तापमान, बाढ़ और सूखे की वजह से 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, जैसे-जैसे हालात बिगड़ेंगे यह नुकसान और बढ़ेगा।
इन छोटी पहल से सुधरेंगे हालातरिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर नीतियां बनाने के साथ आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए खर्च बढ़ाना होगा। समाज की मुख्यधारा से कटे समुदायों को मुख्यधारा में लाना होगा। माइग्रेशन रोकने के लिए भी पॉलिसी बनानी होगी। आपदाओं से निपटने का प्रबंध करने के साथ रोजगार, सबको शिक्षा, सेहत, मातृत्व सुरक्षा और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को बेहतर और सर्वसुलभ बनाना होगा। जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके लिए और आपदा से पीड़ित क्षेत्रों के लिए नौकरी के अवसर बनाने होंगे। विकसित देशों को कर्ज की बजाय क्लाइमेट फाइनेंस अनुदान के रूप में अधिक राशि देनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है, जिससे होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सके। गरीब तबके के लोगों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि दक्षिण एशिया में माइग्रेशन रोकने के लिए उठाने होंगे ठोस कदम उठाए जाएं। इसके लिए अमीर देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अमीर मुल्कों को दक्षिण एशियाई मुल्कों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं पर लगाम लगाने के लिए प्लान तैयार करने समेत सभी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
जलवायु परिवर्तन को लेकर तैयारीभारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए मजबूत आर्थिक विकास की आवश्यकता है। जरूरी है कि ये विकास समावेशी और सतत विकास को ध्यान में रख कर किया जाए। भारत की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर वैश्विक औसत से कम है। ये काफी सकारात्मक पहलू है। लेकिन हमें आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए एक खास रणनीति की जरूरत है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर देश की क्षमता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन करना निश्चित किया गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि नवंबर 2024 तक, देश में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 46.8% बिजली उत्पादन हो चुका है। कोयला से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करने के बजाय, भारत सुपर-क्रिटिकल , अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल , और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है।
चरम मौसम की घटनाओं में होगा ईजाफाविश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 प्रतिशत संभावना है कि अगले पांच वर्षों में से किसी एक साल औद्योगिक युग की शुरुआत की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1.5°C से अधिक तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन के कहीं अधिक गंभीर प्रभाव और एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स जोखिम पैदा होंगे। तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी से भी मौसम में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि पेरिस समझौते के तहत, देशों ने दीर्घकालिक वैश्विक औसत सतही तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से नीचे रखने और इस सदी के अंत तक इसे 1.5°C तक सीमित रखने के प्रयासों पर सहमति जताई है।
डब्ल्यूएमओ की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2028 के बीच हर साल के लिए वैश्विक औसत सहती तापमान 1850-1900 की आधार रेखा से 1.1 डिग्री सेल्सियस और 1.9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होने का अनुमान है। यूनाइटेड नेशन इनवायरमेंट प्रोग्राम के पूर्व निदेशक रहे राजेंद्र माधवराव शेंडे कहते हैं नासा की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच हर महीने औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहा। वहीं इस साल मई का महीने अब तक के सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया है। ये रिपोट्स बताती हैं कि आने वाले दिनों में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़, सूखा, पीने के पानी कि किल्लत, चक्रवात और हीटवेव जैसी घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ग्लेशियर के तेजी से गलने से एक तरफ जहां बाढ़ जैसी स्थितियां बनेंगी वहीं समुद्र के स्तर में भी वृद्ध देखी जाएगी। इन सब हालातों के बीच सबसे बड़ी चुनौती खाद्य सुरक्षा को सुनश्चित करना होगा। क्योंकि मौसम में बदलाव से फसल चक्र पर भी असर होगा। वहीं अचानक तेज बारिश जा सूखे जैसे हालात से भी फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी।
बढ़ती गर्मी साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए मुश्किल बढ़ेगी। इन हालातों को देखते हुए हमें अभी से तैयारियां तेज करनी होंगी हमें फसलों के ऐसे बीज तैयार करने होंगे जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। वहीं हमें ऐसी फसलें विकसित करनी होंगी जो बेहद कम पानी में बेहतर उत्पादन कर सकें। वहीं हमें विकास के मॉडल भी पर्यावरण को ध्यान में रख कर बनाने होंगे। हमें इस तरह के घर बनाने होंगे जिनमें कम गर्मी हो, हमें हरियाली को बढ़ाना होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर भी लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।